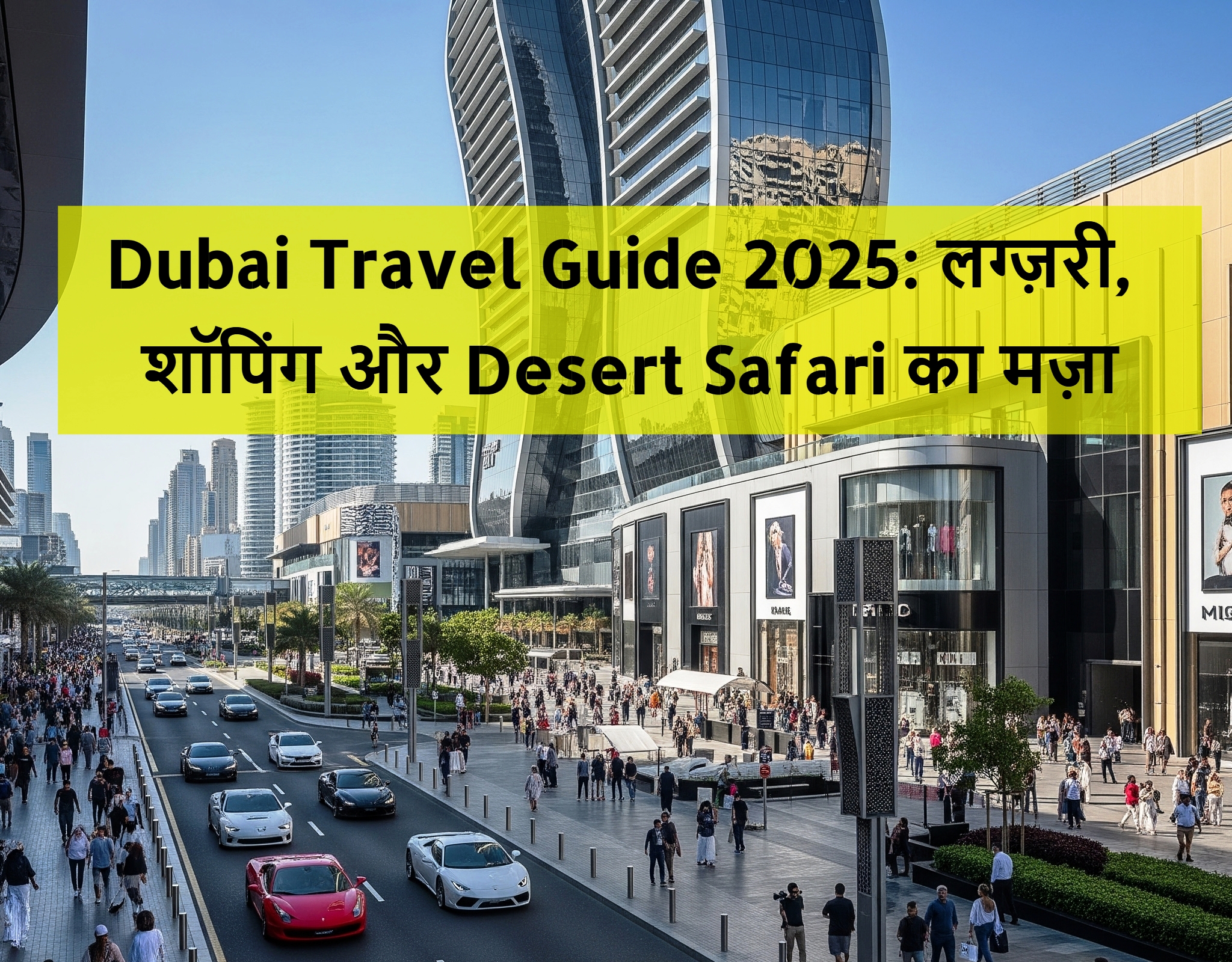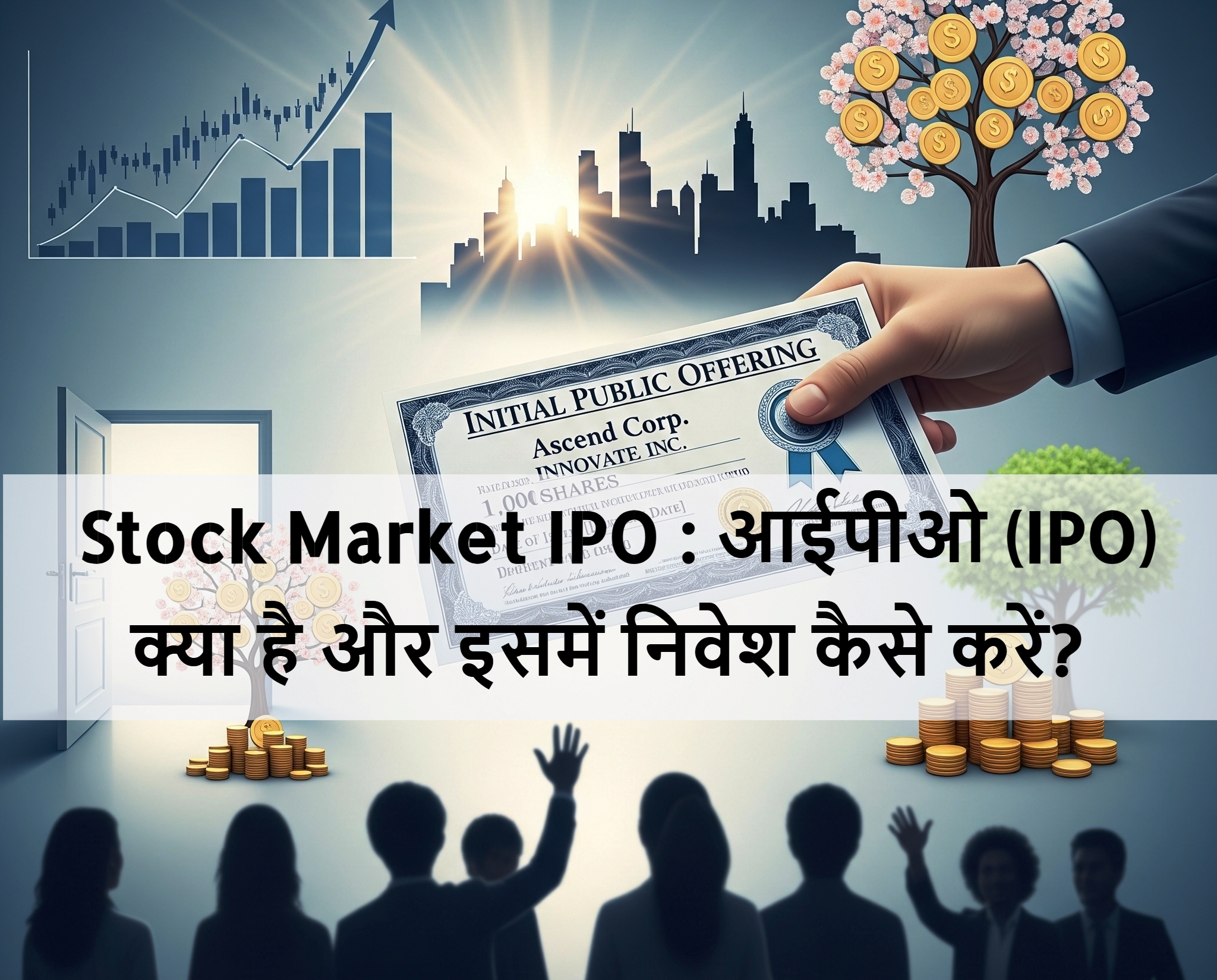SCO Summit 2025 : 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक, चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। यह आयोजन न केवल संगठन के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन था, बल्कि यह वैश्विक भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुआ। इस शिखर सम्मेलन में 10 सदस्य देशों—चीन, भारत, रूस, ईरान, पाकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और ताजिकिस्तान—के साथ-साथ 20 से अधिक देशों के नेताओं और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस लेख में हम इस शिखर सम्मेलन के महत्व, इसकी प्रमुख उपलब्धियों, और इसके वैश्विक प्रभावों पर चर्चा करेंगे।
SCO Summit का ऐतिहासिक संदर्भ
SCO Summit 2025 : शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में हुई थी। यह संगठन मूल रूप से “शंघाई फाइव” (चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और ताजिकिस्तान) से विकसित हुआ, जिसका गठन 1996 में सीमा विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था। 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के साथ यह औपचारिक रूप से एससीओ बन गया, और बाद में भारत, पाकिस्तान, ईरान, और बेलारूस जैसे देश इसके पूर्ण सदस्य बने। वर्तमान में, संगठन में 10 पूर्ण सदस्य देश, दो पर्यवेक्षक देश (अफगानिस्तान और मंगोलिया), और 14 संवाद भागीदार हैं।
एससीओ का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, और आतंकवाद, अलगाववाद, और उग्रवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करना है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है, और क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) ताशकंद, उज्बेकिस्तान में स्थित है। संगठन का “शंघाई स्पिरिट” सिद्धांत—पारस्परिक विश्वास, समानता, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, और साझा विकास—इसके कार्यों का आधार है।
तियानजिन शिखर सम्मेलन 2025: एक अवलोकन
तियानजिन में आयोजित 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 को “एससीओ सतत विकास वर्ष” के रूप में नामित किया गया था। यह आयोजन तियानजिन के मीजियांग कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र में हुआ, जिसे विशेष रूप से इस अवसर के लिए नवीनीकृत किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में 998 युवा स्वयंसेवकों ने अतिथि स्वागत, पंजीकरण, और सामग्री वितरण जैसे कार्यों में योगदान दिया।
शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की, और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और अन्य प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और आसियान महासचिव काओ किम हॉर्न जैसे अंतरराष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को वैश्विक महत्व प्रदान किया।
प्रमुख चर्चाएँ और उपलब्धियाँ
1. तियानजिन घोषणापत्र
शिखर सम्मेलन में “तियानजिन घोषणापत्र” को अपनाया गया, जो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक एकीकरण, और सतत विकास पर केंद्रित था। इस घोषणापत्र ने आतंकवाद, अलगाववाद, और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दोहराया। विशेष रूप से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के पहलगाम हमले (22 अप्रैल 2025) का उल्लेख करते हुए आतंकवाद के वित्तपोषण और कट्टरपंथ के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आह्वान किया।
2. 2035 तक एससीओ विकास रणनीति
सदस्य देशों ने 2035 तक की एससीओ विकास रणनीति को मंजूरी दी, जिसमें व्यापार और निवेश बाधाओं को कम करने, क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं को विकसित करने, और गैर-अमेरिकी मुद्रा आधारित व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। चीन ने इस रणनीति के लिए 2 अरब युआन (लगभग 280 मिलियन डॉलर) की मुफ्त सहायता और 10 अरब युआन की ऋण सुविधा की घोषणा की।
3. आतंकवाद विरोधी सहयोग
एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) को और मजबूत करने पर सहमति बनी। यह संरचना खुफिया साझा करने, संयुक्त सैन्य अभ्यास, और आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत ने इस मंच का उपयोग आतंकवाद के खिलाफ अपनी “शून्य सहनशीलता” नीति को रेखांकित करने के लिए किया।
4. आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग
शिखर सम्मेलन में डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), और सतत विकास पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। 11 जुलाई 2025 को तियानजिन में आयोजित डिजिटल अर्थव्यवस्था मंच में 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 16 जुलाई को शीआन में दूसरा एससीओ राष्ट्रीय टेलीविजन महोत्सव आयोजित किया गया।
5. वैश्विक सुशासन पहल
शी जिनपिंग ने “वैश्विक सुशासन पहल” (GGI) का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार करना है। यह पहल वैश्विक दक्षिण के देशों के हितों को बढ़ावा देने और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित थी।
भारत की भूमिका और रुख
भारत ने इस शिखर सम्मेलन में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उपस्थिति के माध्यम से भारत की सामरिक स्वायत्तता और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ रुख को रेखांकित किया। उन्होंने तीन स्तंभों—सुरक्षा, कनेक्टिविटी, और अवसर—के तहत भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की मांग की और विशेष रूप से पहलगाम हमले का उल्लेख किया, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे।
हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस शिखर सम्मेलन में भी स्पष्ट था। भारत ने अप्रैल 2025 में कश्मीर में हुए आतंकी हमले को संयुक्त बयान में शामिल न करने पर आपत्ति जताई, जिसे पाकिस्तान के पक्ष में माना गया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद पर अपनी चिंताओं को दस्तावेज में शामिल करना चाहता था, जो एक विशेष देश को स्वीकार्य नहीं था।
वैश्विक भू-राजनीतिक प्रभाव
यह शिखर सम्मेलन वैश्विक भू-राजनीति में कई मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, यह चीन और रूस के नेतृत्व में वैश्विक दक्षिण के लिए एक मंच के रूप में उभरा, जो अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था का विकल्प प्रस्तुत करता है। दूसरा, भारत और पाकिस्तान जैसे परस्पर विरोधी हितों वाले देशों की उपस्थिति ने संगठन की एकता और प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। तीसरा, म्यांमार जैसे गैर-सदस्य देशों की भागीदारी ने संगठन के विस्तार की संभावनाओं को उजागर किया।
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
एससीओ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत-पाकिस्तान तनाव और किर्गिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा विवाद जैसे द्विपक्षीय मुद्दों ने संगठन की एकता को प्रभावित किया है। कुछ भारतीय विश्लेषकों ने इसे “शंघाई विरोधाभास संगठन” करार दिया, क्योंकि सदस्य देशों के बीच व्यापक मतभेद हैं। इसके अलावा, रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान-इजरायल तनाव जैसे वैश्विक संघर्षों में एससीओ की तटस्थता ने इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं | तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 ने संगठन की वैश्विक प्रासंगिकता को रेखांकित किया। यह न केवल क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का मंच था, बल्कि यह वैश्विक दक्षिण के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत करने का प्रयास भी था। भारत की सक्रिय भागीदारी ने इसकी सामरिक स्वायत्तता को प्रदर्शित किया, जबकि आतंकवाद और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर इसकी दृढ़ता ने संगठन के भीतर इसकी स्थिति को मजबूत किया। हालांकि, संगठन को अपने सदस्यों के बीच एकता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना होगा। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक मंच पर एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।